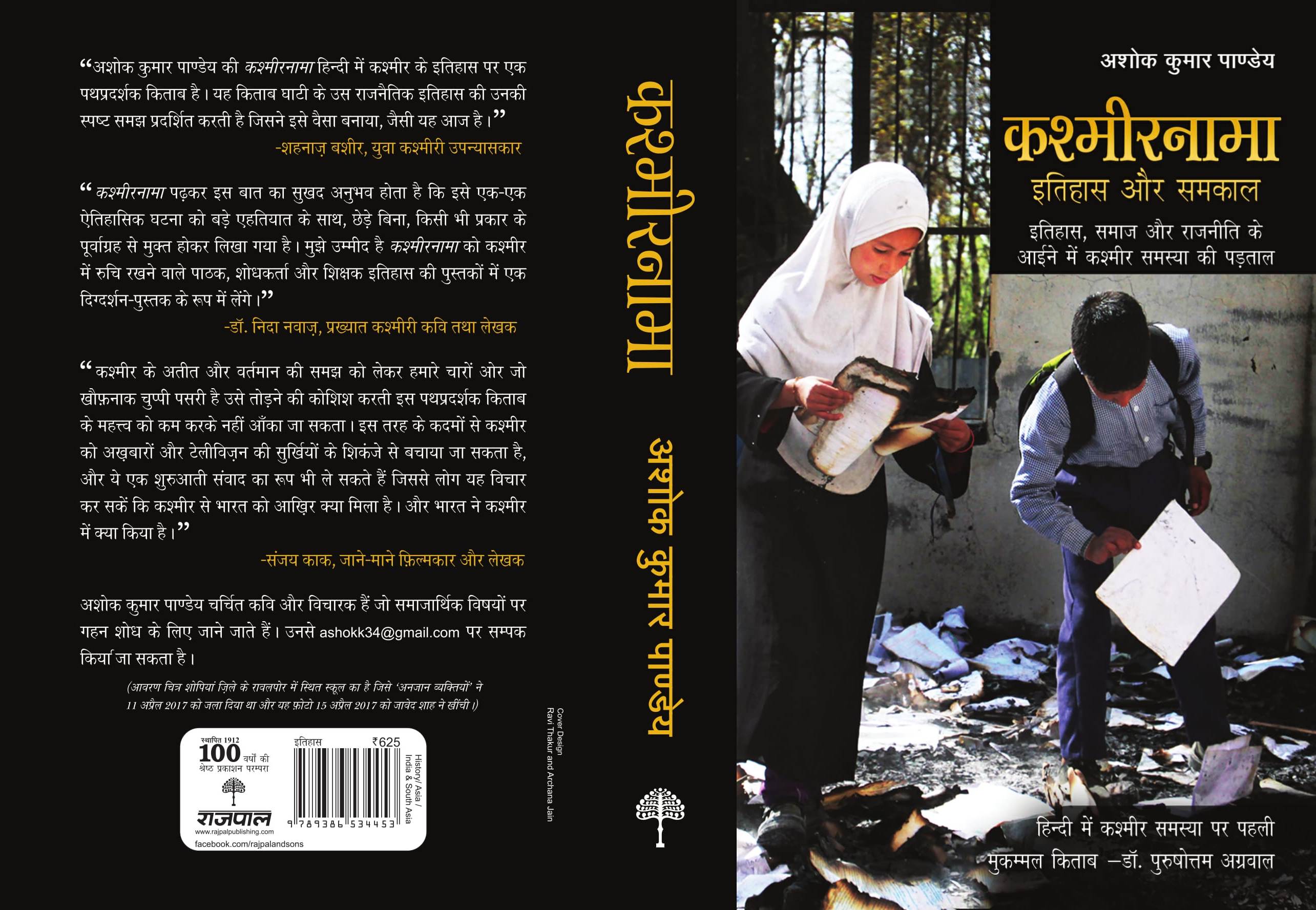
हिंदी में किताबें तो बहुत छपती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी होती हैं जो हिंदी जगत की ‘दरिद्रता ‘ दूर करती हैं या कर सकती हैं। कवि-लेखक अशोक कुमार पाण्डेय की कश्मीरनामा : इतिहास और समकाल इसी सिलसिले की किताब है जो छपने के पहले ही चर्चित हो चुकी है। इसे लेकर अशोक पिछले कुछ सालों से जैसा श्रम कर रहे हैं, वह फे़सबुक के ज़रिए सामने आए किताब के अंशों से पता चलता है। 6 जनवरी से शुरू हो रहे पुस्तक मेले में यह किताब उपलब्ध होगी। किताब की सामग्री को प्रकाशन-पूर्व देख चुके लोगों के मुताबिक सौ से अधिक किताबों और दस्तावेज़ों में फैली सामग्री को एक जगह पेश करने वाली इस बेहद तथ्यपूर्ण किताब ने एक बड़ी कमी पूरी की है। हिंदी जगत में कश्मीर के इतिहास और वर्तमान को लेकर फैले तमाम भ्रमों को यह किताब दूर करेगी। जो लोग कश्मीर के नाम पर खीर और चीर का तुक भिड़ाने लगते हैं, उन्हें पता चलेगा कि कश्मीर दरअसल एक पीर है जो पर्वत बन गई। पेश है किताब का एक अंश-संपादक
 नब्बे के दशक के आख़िरी वर्ष और इस सदी के पहले डेढ़ दशकों में तमाम कोशिशों के बावज़ूद कश्मीर के हालत बहुत सुधरे नहीं. देश के भीतर साम्प्रदायिक तनाव के उभार और सैन्य विचारधारा के प्रभावी होते जाने के साथ-साथ कश्मीर में भी जो बदलाव आये उन्होंने तमाम सकारात्मक कोशिशों पर पानी फेर दिया. यहाँ मेरी कोशिश संक्षेप में इन डेढ़ दशकों के किस्से के ज़रूरी पहलू बयान कर देने की है.
नब्बे के दशक के आख़िरी वर्ष और इस सदी के पहले डेढ़ दशकों में तमाम कोशिशों के बावज़ूद कश्मीर के हालत बहुत सुधरे नहीं. देश के भीतर साम्प्रदायिक तनाव के उभार और सैन्य विचारधारा के प्रभावी होते जाने के साथ-साथ कश्मीर में भी जो बदलाव आये उन्होंने तमाम सकारात्मक कोशिशों पर पानी फेर दिया. यहाँ मेरी कोशिश संक्षेप में इन डेढ़ दशकों के किस्से के ज़रूरी पहलू बयान कर देने की है.
भारत सरकार की ओर से कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने और बातचीत द्वारा मुद्दे को हल करने की पहली कोशिश 4 नवम्बर 1995 को हुई जब पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंहाराव ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा-
पिछले छः सालों में कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद के चलते अभूतपूर्व कष्ट सहे हैं. लोगों ने अकथ हिंसा झेली है जो मौतों और तबाही में तब्दील हुई है. हज़ारों लोग अपने घर-परिवार से उखाड़ दिए गए हैं. यह आभासी छद्म युद्ध सीमा पार से छेड़ा गया है जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों, अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों और मानवीय व्यवहार तथा शिष्टाचार के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है…जम्मू और कश्मीर राज्य और उसके निवासी भारत के वैविध्यपूर्ण अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है. इसलिए हम उनके कष्टों के मूकदर्शक नहीं हो सकते. पहले ही उन्होंने बहुत सहा है. हम राज्य में सामान्य स्थिति लाने का और हर आँख से आँसू पोछ देने का अपना संकल्प ज़ाहिर करते हैं.
इसी भाषण में उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें 370 को जारी रखने, भारतीय संविधान के तहत स्वायत्ता देने और सदर ए रियासत तथा वज़ीर ए आज़म का संबोधन फिर से देने, राज्य के लिए राजनैतिक तथा आर्थिक पैकेज के साथ-साथ राज्य का विभाजन न करने तथा शेख़ अब्दुल्ला और इंदिरा गाँधी के बीच हुए कश्मीर समझौते के तहत आगे बढ़ने की बात थी. हालाँकि इसे लेकर कश्मीर में कोई सकारात्मक माहौल नहीं बना और यह नेशनल कॉन्फ्रेंस तक को प्रभावित करने में असफल रहा लेकिन इसने आगे बढ़ने का रास्ता तो खोला ही. दुलत बताते हैं कि नरसिंहाराव शब्बीर शाह को कश्मीर चुनावों में हिस्सा लेने के लिए राज़ी करना चाहते थे. यह दिल्ली की किसी अलगाववादी नेता को मुख्यधारा में लाने की पहली कोशिश थी. लेकिन शब्बीर के टालमटोल के चलते यह संभव नहीं हुआ. (दुलत-75-77) नरसिंहा राव के पास बहुत समय था भी नहीं. मई 1996 के चुनावों में कांग्रेस हार गई. जम्मू और कश्मीर में इस चुनाव का व्यापक पैमाने पर बहिष्कार हुआ. लेकिन उसी साल जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और राष्ट्रपति शासन के लम्बे दौर का अंत हुआ. देश की नई गठबंधन सरकार ने नवम्बर 1996 में राज्य की आतंरिक स्वायत्ता को परिभाषित करने के लिए एक राज्य स्वायत्ता कमेटी बनाई जिसका अध्यक्ष करण सिंह को बनाया गया. कमेटी शुरू से ही विवादों में रही. अब्दुल्ला परिवार और करण सिंह की अनबन जगज़ाहिर थी. मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला पर हस्तक्षेप का आरोप लगाकर करण सिंह ने अगस्त, 1997 में इस्तीफ़ा दे दिया तो क्षेत्रीय स्वायत्ता पर बनी एक उप समिति के अध्यक्ष बलराज पुरी को समिति से हटा दिया गया. वर्ष 2000 में जब समिति की रिपोर्ट आई तो केंद्र में बाजपेयी की सरकार आ चुकी थी. राज्य विधानसभा से पारित इस रिपोर्ट को एन डी ए की सरकार ने खारिज़ कर दिया. असल में सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस रिपोर्ट से कोई ख़ुश नहीं था, न बाजपेयी, न जम्मू और कश्मीर का विपक्ष और न ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस.
बाजपेयी का दौर कश्मीर के संदर्भ में सबसे बेहतर दौरों में से एक माना जाता है. हिंसा और दमन की जगह इस दौर में मरहम और बातचीत की राह अपनाई गई और उसके सकारात्मक परिणाम भी निकले. इस रिपोर्ट के खारिज़ होने से नाराज़ होने के बावज़ूद फ़ारूक़ ने इस बार जल्दबाज़ी से काम नहीं लिया और स्वायत्ता की मांग जारी रखते हुए अपनी पार्टी को एन डी ए का हिस्सा बनाये रखा. जुलाई 2000 में बेग़म अकबर जहाँ की मृत्यु पर जब बाजपेयी और आडवाणी मातमपुर्सी के लिए श्रीनगर पहुँचे तो रिपोर्ट खारिज़ होने से फ़ारूक़ और दिल्ली के बीच जमी बर्फ़ पिघलना शुरू हुई. कश्मीर समस्या के समाधान तथा पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने के प्रति अपनी रूचि बाजपेयी पहले ही प्रकट कर चुके थे. 1998 में वह बस से लाहौर गए और 1999 की शुरुआत में ही हुई लाहौर घोषणा में दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाने की बात की थी. लेकिन 1999 की गर्मियों में कारगिल में पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पार कर दोनों देशों के बीच एक और युद्ध को जन्म दिया. नवाज़ शरीफ़ इसके लिए मुशर्रफ़ को ज़िम्मेदार ठहराते हैं तो अपनी किताब ‘इन द लाइन ऑफ़ फायर’ में मुशर्रफ़ ने अलग ही क़िस्सा सुनाते हुए नवाज़ शरीफ़ को इसका ज़िम्मेवार बताया है. उस पर विस्तार से बात करना यहाँ विषयांतर होगा. कारगिल में पाकिस्तान को निर्णायक शिक़स्त देने के बाद बाजपेयी सरकार ने सीधे कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से बात करने का निश्चय किया जिसका उन्हें उचित प्रतिसाद भी मिला. पेट्रीयाट के पूर्व संपादक आर के मिश्रा, एस के दुलत और वजाहत हबीबुल्ला के ज़रिये कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत की यह कोशिश निश्चित रूप से दिल्ली की कश्मीर नीति में एक पैराडाइम शिफ्ट थी जो अब तक हुर्रियत को पाकिस्तानी एजेंट से अधिक महत्त्व देने को तैयार नहीं था. इस बातचीत का सीधा कोई फ़ायदा हुआ हो या नहीं लेकिन यह तथ्य तो निर्विवाद है कि दोनों देशों के परमाणु बम बना लेने की क्षमता हासिल कर लेने, कारगिल युद्ध, संसद पर हमले, आगरा में बातचीत विफल होने और ऐसी तमाम घटनाओं के बावज़ूद यह दौर कश्मीर के हालिया इतिहास में सबसे शांत दशकों में से एक था. हालाँकि एन एन वोहरा को वार्ताकार बनाने के बावज़ूद हुर्रियत से बातचीत के लिए न भेजने से वाजपेयी द्वारा अप्रैल 2003 में श्रीनगर में ‘इंसानियत’ के आधार पर कश्मीर समस्या का हल ढूँढ़ ने का प्रस्ताव बस प्रस्ताव ही रह गया तो वादे के बावज़ूद फ़ारूक़ को उपराष्ट्रपति पद न देने से एक अविश्वास का माहौल भी बना.
ऐसा नहीं है कि इस दौर में आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो गया था. लेकिन जो बड़ा परिवर्तन आया था वह था लोगों का आतंकवाद के प्रति मोहभंग. इसीलिए आतंकवादियों ने इस दौर में अपनी रणनीति बदली. कारगिल युद्ध के बाद 1999 से 2003 के बीच उन्होंने फिदाईन या आत्मघाती हमलों की नीति अपनाई. 1999 के मध्य से 2002 के अंत तक ऐसी कम से कम 55 घटनाएँ हुईं जिनमें सुरक्षा बलों के 161 लोग और 90 फिदायीन मारे गए. इन फिदाईनों में अधिकांश लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से घुसपैठ करके आये आतंकवादी थे. नवम्बर-2008 में मुंबई के ताज होटल पर हुआ हमला इस तरह से किये गए हमलों की आख़िरी कड़ी था. यह 1990-1995 की युद्ध जैसी स्थितियों से अलग स्थिति थी और श्रीनगर पहले की तुलना में काफी सामान्य था. पर्यटक एक बार फिर घाटी का रुख करने लगे थे और व्यापार के लिए बेहतर स्थितियाँ बन रही थीं. 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान के लिए आतंकवादी संगठनों की मदद मुश्किल होते जाने के साथ ही कश्मीर फिदाइन हमलों की घटनाएँ लगभग बंद हो गईं.
लेकिन संघ परिवार बाजपेयी के इन प्रयासों से ख़ुश नहीं था. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मशताब्दी वर्ष में गुजरात के गाँधीनगर में हुई आर एस एस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में जम्मू और कश्मीर के लिए स्वायत्ता के किसी प्रस्ताव का पुरज़ोर विरोध किया गया तो बाला साहब ठाकरे ने भी सुर में सुर मिलाया. यही वज़ह थी कि मंत्रिमंडल ने वह प्रस्ताव खारिज़ कर दिया था. नूरानी आगरा वार्ता की असफलता का आरोप पार्टी में हार्डलाईनर माने जाने वाले तत्कालीन गृहमंत्री अडवाणी पर लगाते हैं तो आर एस एस तथा बजरंग दल जैसे संगठन उस पूरे दौर में कश्मीर को लेकर जो भाषा बोल रहे थे वह सरकार की भाषा से भिन्न थी. यही नहीं, 2005-06 में जब मनमोहन सिंह और परवेज़ मुशर्रफ़ कश्मीर समस्या के समाधान के बहुत क़रीब थे, तब भाजपा ने उनका सहयोग करने की जगह बाधाएँ पहुँचाई. 25 जनवरी, 2004 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने मनमोहन सिंह की नीतियों की तीख़ी आलोचना की तो कभी हुर्रियत से बातचीत की पहल करने वाले बाजपेयी ने मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में आश्चर्यजनक रूप से तीन आरोप लगाए, पहला शान्ति प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कश्मीर केन्द्रित हो गई है, दूसरा यह आतंकवाद पर ख़ामोश है और तीसरा हुर्रियत को महत्त्व दिया जा रहा है! तो कश्मीर को लेकर नीतियों को सर से पैर तक पर खड़ा करने की क़वायदें चलती रहीं.
इसी बीच 2002 में जम्मू और कश्मीर में चुनाव हुए. हुर्रियत नेताओं ने इसके बहिष्कार की अपील की लेकिन साथ ही न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने की अपील भी की बल्कि अपने कुछ लोगों को निर्दलीय चुनाव भी लड़वाया. वैसे तो इन चुनावों में आतंकवादी हमलों में 87 राजनैतिक कार्यकर्ता मार दिए गए जो पिछले चुनावों की तुलना में सबसे बड़ी संख्या थी लेकिन चुनावों की घोषणा से पहले ही कश्मीर के प्रमुख अलगाववादी नेता तथा कश्मीर समस्या के हल के भारत से बातचीत के पक्षधर अब्दुल ग़नी लोन की हत्या कर दी गई. वह 1990 में मीरवायज़ मौलवी फ़ारूक़ के बाद मारे जाने वाले पहले बड़े अलगाववादी नेता थे. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता लोन उग्रपंथी रुख के तीख़े आलोचक थे. उनका मानना था कि हिंसा से कश्मीर समस्या नहीं सुलझाई जा सकती. मीडिया में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि लोन चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं. ऐसे समय में जब अटल बिहारी बाजपेयी कश्मीर आने वाले थे और बातचीत की उम्मीदें फ़िज़ा में थीं, लोन की हत्या ज़ाहिर तौर पर इन उम्मीदों में ख़लल पहुँचाने की साजिश थी. फ़ारूक़ ने इसका इलज़ाम पाकिस्तान पर लगाया. अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट कॉलिन पॉवेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “हालाँकि किसी ने उनकी हत्या का जिम्मा नहीं लिया है लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके हत्यारे उनमें से ही हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो. 2 जनवरी 2011 को विभाजित हुर्रियत के नरमपंथी धड़े के मुख्य प्रवक्ता अब्दुल गनी बट्ट ने एक कार्यक्रम में स्वीकार किया मीरवायज़ मौलवी फ़ारूक़, अब्दुल ग़नी लोन और जे के एल ऍफ़ के विचारक प्रो. अब्दुल ग़नी वानी की हत्या भारतीय सेना ने नहीं बल्कि किसी अन्दर के व्यक्ति ने की थी. कश्मीर आन्दोलन में बुद्धिजीवियों की भूमिका पर आयोजित इस सेमीनार में उन्होंने कहा- “हमने अपने बुद्धिजीवियों को मार डाला. जहाँ भी हमें कोई बुद्धिजीवी मिला, हमने उसे मार डाला. ” कश्मीरी आत्मनिर्णय के सवाल के बीच पाकिस्तान के हस्तक्षेप ने उस सवाल को कितना “कश्मीरी” रहने दिया है, यह विचारणीय सवाल है. इस लम्बे संघर्ष में एक एक करके हर उस आवाज़ को दबा दिया गया जिसने पाकिस्तान में विलय से अलग लाइन ली. भारत ऐसे लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान कर सका और ऐसी घटनाओं के बाद माहौल को अपने प्रति संवेदनशील क्यों नहीं बना सका, यह एक और बड़ा सवाल है. कश्मीर के हालात ऐसे ही अनुत्तरित सवालों की पैदाइश हैं.
इन चुनावों में लगभग 45 प्रतिशत मतदान हुआ और आश्चर्यजनक रूप कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 20 सीटें जीतीं. पी डी पी को 16 सीटें मिलीं. नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी. लेकिन कांग्रेस ने पी डी पी का साथ चुना और इस तरह न केवल मुफ़्ती का कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न अंततः कांग्रेस के सहारे ही पूरा हुआ बल्कि आज़ादी के बाद पहली बार कश्मीर में सत्ता चुनावों से बदली.
कांग्रेस और पीडीपी के बीच 3-3 साल तक सत्ता में रहने का समझौता हुआ था और इसके तहत 2005 में ग़ुलाम नबी आज़ाद कश्मीर के मुख्यमंत्री बने. दोनों दलों के बीच पहली दरार तब पड़ी जब पीडीपी के एक विधायक मुर्तज़ा खान ने एक निजी बिल प्रस्तुत किया जिसमें जम्मू और कश्मीर की लड़कियों को बाहरी व्यक्ति से शादी करने पर संपत्ति के अधिकार तथा नागरिकता से वंचित करने का प्रस्ताव था. यहाँ पाठकों को 2002 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का वह फ़ैसला याद होगा जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि राज्य की महिलाओं की नागरिकता किसी भी पुरुष से विवाह करने सुरक्षित रहेगी. 6 मार्च 2004 को क़ानून मंत्री मुज़फ्फ़र बेग़ ने विधानसभा में इस आशय का बिल प्रस्तुत किया. लेकिन कांग्रेस ने इस बिल पर सहमति देने से इंकार कर दिया और अंततः यह बिल पास न हो सका. ग़ुलाम नबी आज़ाद के पदग्रहण के बाद उभरे अमरनाथ श्राइन बोर्ड विवाद ने गठबंधन में दरारें और गहरी कर दीं.
अमरनाथ का ज़िक्र छठी शताब्दी मे लिखे नीलमत पुराण से लेकर कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी मे भी पाया जाता है जहाँ यह कथा नाग शुर्श्रुवास से जुड़ती है जिसने अपनी विवाहित पुत्री के अपहरण का प्रयास करने वाले राजा नर के राज्य को जला कर खाक कर देने के बाद दूध की नदी जैसे लगने वाली शेषनाग झील मे शरण ली और कल्हण के अनुसार अमरेश्वर की तीर्थयात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को इसका दर्शन होता है। सोलहवीं सदी मे कश्मीर आए फ्रेंकोइस बर्नियर के यहाँ भी इसका वर्णन मिलता है और संभवतः सत्रहवीं सदी तक यह यात्रा जारी रही थी। आधुनिक काल मे कोई डेढ़ सौ साल पहले एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने इस गुफा को फिर से तलाशा तथा आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर श्रावण पूर्णिमा के बीच मे बड़ी संख्या मे यात्रियों का गुफा मे निर्मित हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए जाना शुरू हुआ। 1991-95 के बीच कश्मीर मे आतंकवाद के चरम स्थितियों के अलावा यह यात्रा लगभग निर्बाध रूप से चलती रही है। अक्तूबर 2000 मे राज्य के तत्कालीन पर्यटन मंत्री एस एस सलातिया ने यात्रा के प्रबंधन के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के निर्माण का विधेयक प्रस्तुत किया और फरवरी 2011 मे राज्य सरकार ने बोर्ड का गठन कर दिया। 2004 मे बोर्ड ने पहली बार बालटाल और चंदनवाड़ी मे जंगलात विभाग के अधीन 3642 कैनाल ज़मीन की मांग की और अगले तीन वर्षों तक मामला जंगलात विभाग, हाईकोर्ट और श्राइन बोर्ड के बीच कानूनी टकरावों मे फंसा रहा।
अमरनाथ यात्रा को लेकर विवाद 2008 मे शुरू हुआ जब ग़ुलाम नबी आज़ाद ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को लगभग 800 कैनाल (88 एकड़) ज़मीन देने का निर्णय लिया और यात्रा के बीच मे ही 17 जुलाई 2008 को राज्यपाल के मुख्य सचिव तथा श्राइन बोर्ड के तत्कालीन सी ई ओ अरुण कुमार ने एक प्रेस कोन्फ्रेंस मे यह घोषणा कर दी ज़मीन का यह अंतरण स्थाई है। अगले ही दिन यह मामला राजनीतिक बन गया, हुर्रियत के दोनों धड़ों ने इसका विरोध किया तो पीडीपी भी स्थाई भू अंतरण के खिलाफ मैदान मे आ गई. नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीछे नहीं रही और शेख़ परिवार की तीसरी पीढ़ी के उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की, अगर हमारी एक इंच ज़मीन भी किसी बाहरी को दी गई तो हम अपनी ज़िन्दगी क़ुर्बान कर देंगे. दूसरी तरफ़ जम्मू मे भाजपा ने मोर्चा खोल दिया और यह विवाद एक धार्मिक विवाद मे तब्दील हो गया जिसमें हिंसक झड़पों मे कई लोग मारे गए। उधर शिवसेना, भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल तथा नवगठित श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति ने जम्मू से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक दी तो घाटी के दूकानदारों ने चलो मुज़फ्फराबाद का नारा दिया और अंततः 28 जून 2008 को पीडीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लालकृष्ण आडवाणी ने इसे चुनाव मे मुद्दा बनाने की घोषणा की तो कश्मीर मे पीडीपी ने इसका उपयोग अपनी अलगाववादी और कट्टर छवि बनाने मे किया। अलगाववादी नेता शेख़ शौकत अज़ीज़ सहित 21 से अधिक लोगों की जान और ग़ुलाम नबी सरकार की बलि लेने के बाद यह मामला 61 दिनों बाद राज्यपाल द्वारा बनाए गए एक पैनल द्वारा अंतरण को अस्थाई बताने तथा बोर्ड को इस ज़मीन के उपयोग की अनुमति के बाद बंद तो हुआ लेकिन कश्मीर के विषाक्त माहौल मे सांप्रदायिकता का थोड़ा और जहर भर गया।






























