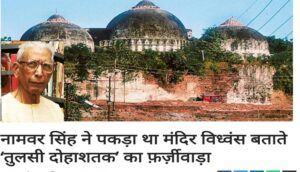पंकज श्रीवास्तव
 सितंबर आते ही ‘राष्ट्रभाषा हिंदी’ का देशव्यापी डंका बजने लगता है।स्वतंत्रता दिवस समारोहों से फ़ारिग सरकार, समाराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सभा-सेमिनारों और हिंदीप्रेमियों की मुफ़्त विदेशयात्राओं के लिए ख़ज़ाना खोल देती है। 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस पर ‘हिंदीसेवियों’ को सम्मानित करने से लेकर नये वादों और इरादों की झड़ी लग जाती है। 2015 में विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा बनाने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी। भोपाल में आयोजित विश्व सम्मलेन में हिंदी का नगाड़ा बजने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस महत्वपूर्ण खोज को सार्वजनिक करने की कृपा भी कर दी थी कि हिंदी ने ‘लड़ने-भिड़ने की भाषा होने की पात्रता’ हासिल कर ली है।
सितंबर आते ही ‘राष्ट्रभाषा हिंदी’ का देशव्यापी डंका बजने लगता है।स्वतंत्रता दिवस समारोहों से फ़ारिग सरकार, समाराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सभा-सेमिनारों और हिंदीप्रेमियों की मुफ़्त विदेशयात्राओं के लिए ख़ज़ाना खोल देती है। 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस पर ‘हिंदीसेवियों’ को सम्मानित करने से लेकर नये वादों और इरादों की झड़ी लग जाती है। 2015 में विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा बनाने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी। भोपाल में आयोजित विश्व सम्मलेन में हिंदी का नगाड़ा बजने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस महत्वपूर्ण खोज को सार्वजनिक करने की कृपा भी कर दी थी कि हिंदी ने ‘लड़ने-भिड़ने की भाषा होने की पात्रता’ हासिल कर ली है।
बहरहाल, हिंदी का यह ‘हासिल’ कम बड़ी क़ामयाबी नहीं, वरना हिंदी आयोजनों में शामिल होने वाले मंच से जो बोलें, उनका दिल अच्छी तरह जानता है कि यह पराजय का जश्न है। 21वीं सदी के भारत में हिंदी का मतलब हो गया है अभाव और दरिद्रता। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी को लेकर जो भी सपना देखा या दिखाया गया हो, आज की सच्चाई यह है कि बिना अंग्रेजी जाने चपरासी और बेयरे की नौकरी मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। दिक़्क़त यह है कि इस ‘अपराध’ में हर रंग के झंडे शामिल हैं। ‘अंग्रेजी को अनिवार्य’ बनाये रखना एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जिस पर वामपंथियों से लेकर दक्षिणपंथियों तक के नेतृत्व में सहमति है। जो समाजवादी पार्टी कभी ‘हिंदी राग’ अलापने के लिए ‘बदनाम’ थी, उसने यूपी में अपनी सरकार रहते, कौशल विकास के विज्ञापनों में ‘अंग्रेजी-दक्ष’ बनाने पर ख़ास ज़ोर दिया। उसने लखनऊ के दिल हजरतगंज का ऐसा कायाकल्प किया कि वहाँ लगभग सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के बोर्ड अंग्रेजी में बदल गए। आज राष्ट्रवादियों की सरकार रहते हिंदी के गढ़प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुख्य बाजार (जहाँ हज़रतगंज चौराहा, अटल चौराहा किया जा रहा है) में हिंदी या उर्दू के साइनबोर्ड को लेकर ‘खोजो तो जाने जैसा खेल खेला जा सकता है।
वैसे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार करते हुए जो व्यवस्था दी थी, वो आज भी कायम है। संविधान के अनुच्छेद 351 में साफ कहा गया है कि ‘संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।’ इससे पहले 24 अप्रैल 1949 को फ्रेंक एन्टनी ने अंग्रेजी को आठवीं सूची में रखने का निजी प्रस्ताव पेश किया तो जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट विरोध करते हुए कहा-‘मैं भूल नहीं सकता कि मुझे चालीस करोड़ जनमानस को अपने साथ रखना है, ना कि कुछ हजार या लाख इलीट को।’
लेकिन समयचक्र ऐसा घूमा कि इलीट की भाषा का डंका बजने लगा। नेहरू की कुर्सी पर बैठने वाले मनमोहन सिंह इंग्लैंड जाकर अंग्रेजों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सिखाई। आठवीं सूची में न होने के बावजूद अंग्रेजी ने देश के हर कोने में जगह बना ली। अंग्रेजी सिखाने का दावा करने वाले स्कूल सुदूर गांवों में खुलने लगे। कस्बों और गांवों के तमाम पेड़ों पर ‘अंग्रेजी स्पोकना सीखें” जैसे बोर्ड लटक गये।
यह एक बड़े संकल्प को उलटने जैसा लगता है लेकिन इसकी ठोस वजह है। दरअसल जनता ने अपने साथ होने वाले ‘छल’ को समझ लिया है। आज़ादी के बाद भारतीय नेतृत्व ने हिंदी का बात तो बहुत की, लेकिन इसमें ज्यादातर भावुकता ही थी। यह सही है कि तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में हिंदी का उग्र विरोध हुआ लेकिन हिंदी प्रदेशों में हिंदी को उसकी जगह दिलाने से किसने रोका था? यह जगह सिर्फ सरकारी साइनबोर्डों में नहीं मिलनी थी। इसका मतलब था इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, वकालत जैसे पेशों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई सुनिश्चित की जाती। हिंदी में ज्ञान-विज्ञान से जुड़े विषयों में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जाता। पर यह सब न करके हिंदी फिल्मों और गानों की धूम को हिंदी की तरक्की के सबूत बतौर दिखाया जाने लगा। ऐसा करने वाले नेताओं और अधिकारियों ने अपने बच्चों को देश-विदेश के महंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षा दिलायी जो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन-प्रशासन की हर महत्वपूर्ण जगह काबिज होते गये।
दुनिया भर के शिक्षाशास्त्री उचित ही मानते हैं कि मातृभाषा के बजाय किसी दूसरी भाषा शिक्षा देना बच्चों के पैर में पत्थर बांधना और मौलिक चिंतन का विकास रोकना है, लेकिन भारतीय शासकवर्ग ने भाषा के मोर्चे पर ऐसा छल किया कि अब जनता यह समझती है कि पैरों में बंधा पत्थर तो हिंदी है। अंग्रेजी तो वह पंख है जिसके सहारे वह दुर्दशा के दलदल से बाहर निकलने की उड़ान भर सकती है। वह भाषा की भावुकता पर और कुर्बान न होकर व्यावहारिक रास्ते पर चलना चाहती है।
महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि अगर वे तानाशाह होते तो ‘हिंदी को शिक्षा के माध्यम के रूप में तुरंत अनिवार्य कर देते, पाठ्यसामग्री बाद में बनती रहती।’ लेकिन अब यह बात उनके लिए भी चुटकुला है जो भारत को तानाशाही के जरिये ही ‘ढर्रे’ पर लाने के विचार को सही ठहराते हैं। ऐसे में यह खुलकर कहने का समय आ गया है कि या तो भारतीय शासकवर्ग हिंदी को अंग्रेजी की जगह स्थापित करने का कोई ठोस और समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करे या फिर ‘राजभाषा’और ‘राष्ट्रभाषा’ के नाम पर होने वाले नाटक को बंद करके अंग्रजी की अनिवार्यता को सार्वजनिक रूप से स्वीकर करे। हिंदी के उत्सव का बजट युद्धस्तर पर अंग्रेजी के प्रचार-प्रसार के लिए खर्च किया जाये। बच्चों को पैदा होने के साथ ही अंग्रेजी की घुट्टी पिलायी जाये ताकि आगे चलकर उनकी सेहत दुरुस्त रहे।
जो लोग हिंदी को आईआईएम, आईआईटी, इसरो,एम्स, सुप्रीम कोर्ट की भाषा बनाने का इरादा नहीं रखते, उनके दावों पर यकीन का कोई मतलब नहीं। उनसे सावधान रहने कि ज़रूरत है। वे ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीज़ के मरने के बाद लाश को वेंटिलेटर पर रख कर घरवालों से वसूली करते रहते हैं। श्मशान में सोहर गाने से जीवन नहीं मिलता !
लेखक मीडिया विजिल के संस्थापक संपादक हैं।